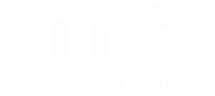एक हुए राही मासूम रज़ा। जिनका किताबों से ख़ास सरोकार नहीं रहा। वो समझ लें कि बीआर चोपड़ा की महाभारत का स्क्रीनप्ले उन्होंने ही लिखा था। उनका एक उपन्यास है ‘आधा गांव’ उस उपन्यास में एक किरदार जब जंग के मोर्चे से अपने गांव वापस जाता है और एक मज़हबी बहस में मजबूर होकर उसे शरीक होना पड़ता है तो वो बड़ी तल्खी लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से कहता है- मोर्चे पर जब मौत सामने होती है तो मुझे अल्लाह तो याद आता है पर सबसे ज़्यादा मुझे अपना गंगौली गांव और घर याद आता है, मुझे काबा याद नहीं आता। वो तो अल्लाह का घर है, वो उसे याद आता होगा.. मुझे तो सिर्फ गंगौली का अपना घर याद आता है।
मरहूम कमलेश्वर आज से 17 साल पहले पाकिस्तान (Pakistan) गए थे। कई शहर घूमे और लौटे तो एक किताब में अपने मनोभाव दर्ज किए। नाम था उसका ‘आंखों देखा पाकिस्तान’। रज़ा के इस किरदार को उन्होंने अपने वहां दिए एक भाषण में याद किया था। अपने इसी भाषण में आगे कमलेश्वर कहते हैं कि- सोचिए, आख़िर इंसान की ये कौन सी बड़ी सच्चाई है जो धर्म मज़हब की सच्चाई से भी बहुत ऊंची उठ सकती है और वह तब, जब मौत जैसी खूंखार सच्चाई उसके सामने खड़ी होती है। आख़िर मौत के आगे कुछ नहीं है, यदि धर्म या मज़हब ही अंतिम सत्य होता तो ‘आधा गांव’ के मुस्लिम पात्र को ‘काबा’ याद आना चाहिए था या किसी हिंदू पात्र को बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, राम या कृष्ण के मंदिर याद आने चाहिए, पर ऐसा निश्चय ही नहीं होता।
कमलेश्वर ने भाषण में कहा था कि जिन कारसेवकों पर अयोध्या में गोली चली उनमें जो ज़िंदा रह गए उन्हें भी अपना गांव-घर याद आया होगा और जो जेहादी सुरक्षाबलों की गोलियों से मारे जाते हैं, उनकी जेब से भी मक्का मदीने की नहीं बल्कि उनके घर-गांव-परिवार की तस्वीरें ही मिलती हैं। शायद कमलेश्वर यकीन दिलाना चाहते थे कि इंसान के पास धर्म तो होता है लेकिन वो कभी उसकी स्मृतियों को फीका नहीं कर पाता। इंसान से उसका घर द्वार नहीं छूटता। अब सवाल है कि मुझे आज ये सब क्यों याद आ रहा है, तो वो आगे बताऊंगा लेकिन पहले एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं जो कमलेश्वर के मित्र हुआ करते थे। बहुत दिलचस्प है उनकी कहानी और खुद कमलेश्वर ने ही सुनाई थी।
उस इंसान का नाम था- तेग इलाहाबादी असल नाम हुआ- मुस्तफा ज़ैदी। तो ज़ैदी साहब जो थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (Allahabad University) में कमलेश्वर से साल भर सीनियर थे। वी.पी. सिंह और चंद्रशेखर इन ज़ैदी साहब के सहपाठी रहे हैं। ये दोनों महानुभाव भारत देश के प्रधानमंत्री हुए लेकिन खुद ज़ैदी साहब भी बहुत हुनरमंद थे। विभाजन के बाद अपने प्रिय शहर में ही टिके रहे। फिर जाने क्या हुआ कि करीब दस साल बाद फैसला लिया कि अब पाकिस्तान में ही रहेंगे। वो चले गए। पाकिस्तानी सरकार ने खूब ख़ैर मकदम किया और सिविल सर्विस की मार्फत एक ऊंची नौकरी दी। आगे चलकर वो कराची के कमिश्नर बनकर रिटायर हुए। अब ज़ैदी ने अपनी अंतिम ज़िंदगी पाकिस्तान में तो बिताई लेकिन उनके ज़हन से इलाहाबाद नहीं मिट सका। शायरी के लिए जिस नाम का इस्तेमाल करते थे वो भी तेग इलाहाबादी ही बना रहा। ज़हन की हलचल समझने के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, उन्होंने लिखा था-
कोई उस देश का मिल जाए तो इतना पूछें
आजकल अपने मसीहा-नफसां कैसे हैं
आंधियां तो सुना उधर भी आईं
कोपलें कैसी हैं शीशों के मकां कैसे हैं!
अपने शहर की याद उन्हें इस कदर सताती थी. आगे लिखा है-
कई समन्दर पार से आई गोरी पिया के देस
रूप विदेशी लेकिन जीवन पूरब का सन्देस
लंबी लंबी पलकें जिन में तलवारों की काट
नीली नीली आंखें जैसे जमुना जी का घाट
अब देखिए कि ज़ैदी साहब भले सिंध, रावी, चिनाब के देश चले गए लेकिन तेग इलाहाबादी ताउम्र जुमना जी के घाटों पर ही बैठा रह गया। यहां वो जमुना भी नहीं लिखते, जमुना जी लिखते हैं। ऐसी होती हैं घर गांव की स्मृतियां और कमलेश्वर कहते थे कि यही तो धर्म की स्मृतियों से ऊपर उठकर संस्कृति बन जाती है।
किसी भी महान संस्कृति के निर्माण में मूल होती है स्मृति। धर्म से भी बहुत ऊंची चीज़। उसकी गोद में तो धर्म खेला करते हैं। पंथ अठखेलियां करते हैं। मत मतांतर से भला उसे क्या फर्क़ पड़ता है। इसी का एक हिस्सा है भाषा। भाषा के माध्यम से हम जाने क्या क्या संजोये रखने में सक्षम हो जाते हैं। आज कमलेश्वर के लिखे की बात चल पड़ी है तो उन्हीं की एक पंक्ति से समझिए। यदि समझ ना आए तो फिर-फिर पढ़िए लेकिन बेपरवाही में छोड़कर आगे मत बढ़िएगा। ये सूत्र कई ताले खोलता है। उन्होंने लिखा है- भाषायी संपदा बताती है कि चाहे कोई भी संस्कृति हो, उसकी धमनियों में धर्म का उन्मादी गंदला रक्त नहीं, स्मृतियों का निरंतर शुद्ध होता उजला रक्त ही प्रवाहित होता है।
इस बात को पुख्ता करते हैं एक और पाकिस्तानी शायर जिनका नाम हुआ अब्दुल अज़ीम ‘खालिद’। ये जनाब रहे उर्दू को सब कुछ मान लेनेवाले पाकिस्तान में लेकिन जाने गए हिंदी शायरी के लिए. खालिद ने पैगंबर के लिए लिखा। लिखा हिंदी में और वो भी कृष्ण के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए। पढ़िए ज़रा चार-छह लाइनें..
तू दीपक मैं काजल तू दरपन मैं सीसा,
मैं कालिख, तू परभात की लालिमा है
जो गोकुल में गोविन्द से फाग खेले,
वे निरलाज नारी नहीं, अप्सरा है
है हके-सिरूह शांति ओम तत्सत्,
अजब दिलकुशा बांसुरी की सदा है
हके-सिरूह को मतलब हुआ सत्य की दैवीय घोषणा। कमाल है कि वो उसमें शांति ओम तत्सत् सुन रहे हैं। ये कमाल है उनकी स्मृति का जो उनको खींच ले गई होगी जालंधर में। खालिद साहब लाहौर में इन्कम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर थे लेकिन शायरी करते रहे। सोचिए कि पाकिस्तान में रहकर एक शख्स पैगंबर के लिए तारीफें लिख रहा है लेकिन उसकी भाषा और प्रतीक कहां से आ रहे हैं? ये सब स्मृति की उपज है। आखिर इंसान जहां पैदा हुआ, जिया, रहा उससे कैसे छूट जाएगा? जब भी उसे अपने मन की बात कहनी होगी तो वो उसी भाषा या प्रतीक में उनको बांधेगा जिनके सबसे करीब खुद को पाएगा।
दरअसल आज एक ख़बर पढ़ी। ख़बर थी हसीना बेगम के बारे में। कौन हैं हसीना बेगम? उन्हें कोई नहीं जानता था। हम सब तब जाने जब वो 18 साल पाकिस्तानी जेलों में कैद रहकर भारत आईं। 26 जनवरी की ही बात है। कभी वो अपने पति के रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गई थीं। वहां उनका पासपोर्ट खो गया तो प्रशासन ने उनको जेल में डाल दिया। तब वो 47 साल की रही होंगी। रिश्तेदारों ने खूब कोशिश की और औरंगाबाद के पुलिस अधिकारियों ने भी मेहनत की। किसी तरह से छूटकर घर पहुंचीं। आईं तो बोलीं मुझे शांति महसूस हो रही है, लग रहा है स्वर्ग में हूं। पंद्रह दिन भी नहीं हुए कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। जब उनके बारे में पढ़ा तो अफसोस हुआ, फिर सुकून आया। अफसोस इसलिए कि उनके 18 साल जेल में गर्क हुए।
सियासत और नौकरशाही इस कदर आम लोगों की ज़िंदगी पर हावी है। सुकून इसलिए कि भले ही 15 दिन सही, मगर उन्होंने अपने घर में सांसें ली होंगी और मरते हुए उनकी आंखें अपना घर नहीं ढूंढ रही होंगी। अपनी हवा-अपनी मिट्टी में होने का मतलब वही जानता है जिसे वो नसीब ना हो। हसीना बेगम शायद अपनी मिट्टी में दफन होने ही चली आई हों। ऐसी चाहतों का मूल वो स्मृति ही तो है जिसकी बात मैं कर रहा था। धर्म, राष्ट्र या राजनीति इसमें दखल दे तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। बाकी सब तर्क है मगर अपना गांव-घर ही मूल है जड़ है। उसके सामने सारे तर्क सारी व्यवस्था चुके हुए हैं। आप क्या सोचते हैं?