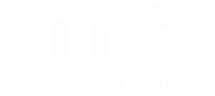मजदूर और जोंक
Editorial: न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 में संशोधन किया जा रहा है। सेक्शन 3(1)(9) में बदलाव किया जा रहा है। संशोधन के अनुसार केन्द्र सरकार पाँच वर्ष में अन्तराल पर न्यूनतम लेबिल फ्लोर वेतन का संशोधन व पुनरावलोकन, गजट में प्रकाशित उपभोक्ता खर्च के आधार पर सकती है। यानि कि मूल्य वृद्धि और मंहगाई दर दिनों दिन बढ़ती रहे, और मजदूर बढ़ती मंहगाई के थपेड़े झेलता हुआ। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए पाँच वर्ष की प्रतीक्षा करता रहे।
पाँच वर्ष बाद भी न्यूनतम मजदूरी में संशोधन होना भी संशयपूर्ण होने के साथ, सरकार की नेकनीयती और प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। भारतीय सरकारें मजदूर को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। ये जगजाहिर है। न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 में प्रस्तावित ये संशोधन मजदूरों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवन्त उदाहरण है। प्रस्तावित संशोधन में न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 का पैराग्राफ 3(1)बी भी स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। जो कि मजदूरों को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि, उनका वेतन कार्य के घण्टे, दिन, मास, या दीर्घतर यानि की समय-सीमा के आधार पर मजदूरी की दर को तय करते थे।
इसके ठीक उल्ट निठल्ले, नाकारा, गप्प हाँकने वाले, चाय पीने, मैच देखने वाले सरकारी कर्मचारियों (कुछ अपवादों को छोड़कर) के लिए, सरकार ने अपने खजाने के पोटलियाँ खोल रखी है। जो अपनी उत्पादकता और काम करने की गुणवत्ता से कहीं ज्यादा वेतन पा रहे है। बात-बात पर नये वेतन आयोग की माँग, मंहगाई भत्ता बढ़ाने की माँग करते है। और हमारी धृतराष्ट्र सरकार इन सरकारी कर्मियों की उत्पादकता और गुणवत्ता से भली-भाँति परिचित होने के बावजूद, इनकी सारी मांगों को सहर्ष शिरोधार्य करती है। एक तरफ खून पसीने बहाने वाला वर्ग, जिस हर क्षण संघर्ष से दो-चार होना पड़ता है। जो अपनी श्रम और उत्पादकता के अनुपात में बेहद मामूली सा वेतन पाता है। वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि, हमारे देश के निज़ाम सरकारी कर्मियों के निठल्ले वर्ग के लिए, जनता का पैसा निरन्तर वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं के नाम पर बहा रहे है। और समय-समय पर वेतन आयोग और महंगाई भत्तों के टुकड़े फेंककर उनका पोषण कर रहे है।
न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 (Minimum Wages Act 1948) के पैराग्राफ 3(1)ए को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव है। इस पैराग्राफ के अनुसार 1000 मजदूरों से कम वाली औद्योगिक इकाइयों में, सरकारों को वेतन तय करने का अधिकार था। लेकिन प्रस्तावित संशोधनों के पारित हो जाने बाद 1000 मजदूरों से कम वाली औद्योगिक इकाइयों में, न्यूनतम वेतन दर तय करने के मामले में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त हो जायेगा। यानि पूंजीपति और औद्योगिक इकाईयों का स्वामित्व रखने वाले लोगों को न्यूनतम वेतन में अनियमिततायें करने की खुली छूट मिल जायेगी।
यानि की लूट करने के स्वर्णिंम अवसर मिलेगें। न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के सैक्शन 8(2) में प्रस्तावित संशोधन में न्यूनतम वेतन के निर्धारण हेतु सरकारों द्वारा अलग-अलग स्तरों पर एडवायजरी बोर्ड या कमेटियों में, मजदूरों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यानि की वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले, सरकारी खर्चों पर पलने वाले, वो लोग जिन्हें श्रमिकों के हितों, उनकी दशाओं, और आवश्यकताओं की बुनियादी समझ नहीं है। वे न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में हिस्सा लेते है। इनके द्वारा निर्धारित किये गये निवाले को पाने के लिए श्रमिक वर्ग अभिशप्त है। भले ही इन निवालों से श्रमिकों का पेट ना भरे। इन बातों से व्यवस्था में बैठे इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। इस प्रस्तावित संशोधन से “जाके पैर ना पड़त बिवाई, ता का जाने पीर पराई” वाली कहावत यथार्थ के धरातल पर उतरती है।
न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के सैक्शन 18(3) के अन्तर्गत जिन संशोधनों की अनुशंसा की गई है। वो श्रमिकों के लिए रक्त चूसक पिस्सुओं का काम करेगें। इसके अन्तर्गत पूंजीपतियों, औद्योगिक इकाईयों का स्वामित्व रखने वाले लोगों को, और औद्योगिक इकाईयों के प्रशासन को मजदूरों से जुड़े दस्तावेज यानि की रिकॉर्ड रजिस्टर, वेतन पर्ची, आदि के रखने की बाध्यता की समाप्त कर दिया गया है।
यानि कि अब मालिक लोगों को शोषण और दोहन करने के लिए सरकारी मान्यता मिल गई है। ऐसे में यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो, मालिकों के पक्ष को शाश्वत सत्य की श्रेणी में रखा जायेगा। भले ही मजदूर अपने हक की आव़ाज को बुलन्द करता रहे। सरकार और मालिकों का बहरापन बना रहेगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 में प्रस्तावित संस्तुतियों में यह निर्धारित किया गया है कि, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का वेतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किये जाने वाले ‘नैशनल फ्लोर लेबिल’ से कम नहीं होगा। लेकिन संस्तुति में ये स्पष्ट नहीं है कि, नैशनल फ्लोर लेबिल का निर्धारण कौन करेगा, इसके मापदण्ड़ क्या होगें, क्या इसमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होगा, यदि होगा तो उसका स्तर क्या होगा। इसमें ये सभी बातें स्पष्ट नहीं है।
जाहिर है, नैशनल फ्लोर लेबिल वेतन का निर्धारण पूंजीपति अपने प्रभाव व धन का इस्तेमाल करते हुए। सत्तानसीं निजामों से करवायेगा। और सरकारों को भी ऐसा करना होगा। अन्यथा पाँच साल बाद होने वाले चुनावों के लिए चन्दा कौन उपलब्ध करवायेगा? आज भले ही सरकार राम-राम और नारायण-नारायण के नाम पर चल रही हो। पर मजदूर रूपी दरिद्रनारायण के जीवन का हाशियाकरण सरकार ने पक्का कर रखा है। सरकारों को इस दिशा में सोचना कोई लाभप्रद सौदा नहीं लगता है। सरकारों का लगता है कि, मजदूर केवल हड़तोड़ मेहनत के लिए और खून पसीना बहाकर उत्पादन करने के लिए ही पैदा होता है। लेकिन सरकारों को ये नहीं मालूम कि रक्त और क्रान्ति का रंग भी लाल होता है।
न्यूनतम वेतन अधिनियम में वेतन संबंधी नियमितताओं में, प्रदेश की भूमिका को समाप्त करने के सशक्त प्रावधान बनाये गये है। जिनके अनुसार न्यूनतम वेतन का ढ़ाँचा तैयार करने में, नैशनल फ्लोर लेबिल का अनुकरण किया जायेगा, यानि की एक केन्द्रीय एकीकृत प्रणाली द्वारा। भारत जैसा विशाल देश जिसमें प्रादेशिक विविधतायें और कई जीवन शैलियाँ है। इसी प्रादेशिक विविधता को आधार बनाते हुए। प्रादेशिक सरकारें अपने राज्य के मजदूरों के लिए तर्कसंगत वेतन दरों का निर्धारण करती है। यदि इस केन्द्रीय एकीकृत वेतन प्रणाली (नैशनल फ्लोर लेबिल वेतन) वाली व्यवस्था को लागू कर दिया जाये तो, ऐसे में पूंजीपति वर्ग चाहेगा या इसकी ज्य़ादा संभावना है कि, पूंजीपति नैशनल फ्लोर लेबिल वेतन दर देश की सबसे कम या औसत मजदूरी वाले राज्यों के आधार पर तय हो।
और उस वेतन दर को ही पूरे देश में लागू किया जाये। साधारण शब्दों में कहा जाये तो, जो मजदूरी दर बिहार व झारखण्ड़ जैसे पिछड़े राज्यों में मजदूरों को मिलती है, वहीं वेतन दर गोवा राज्य के मजदूरों को मिले। जबकि बिहार झारखण्ड़ और गोवा राज्यों के मजदूरों की जीवन शैली और खर्चों में पर्याप्त अन्तर है।
अब बात करते है, फैक्ट्री एक्ट में बदलाव की, प्रस्तावित संशोधन पारित हो जाने के बाद, जिन औद्योगिक संस्थानों में शक्तिचालित (Electrical/Automatic Machine) मशीनों पर काम होता है, वहाँ पर 20 तथा जिन कम्पनियों में हस्तचालित (Manual Machine) मशीनों पर काम होता है, वहाँ पर 40 से कम श्रमिक होने पर, उन औद्योगिक इकाइयों को फैक्ट्री एक्ट के दायरे से बाहर रखा जायेगा, और उन्हें लघु उद्यम का दर्जा दे दिया जायेगा।
जबकि पहले ये संख्या शक्तिचालित औद्योगिक संस्थानों के लिए 10 मजदूर तथा हस्तचालित फैक्ट्रियों के लिए 20 मजदूर थी। अब फैक्ट्री मालिक को इस कानून के पारित होने से बह्मास्त्र मिल जायेगा। यानि की अब वे लोग (फैक्ट्री मालिक) अपने संस्थान में मजदूरों की कम संख्या दिखाकर, फैक्ट्री एक्ट अन्तर्गत आने वाले दायित्वों से साफ बचकर निकल जायेगें। और अपने-अपने संस्थान को छोटे उद्यमों की श्रेणी में दिखाने से गुरेज नहीं करेगें। लघु औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाले लाभ का फायदा उठायेगें। लाभ यानि की लघु उद्यमों को मिलने वाला, कम ब्याज दर का बैंक लोन। इन छोटे औद्योगिक उद्यमों को श्रम कानून पालन संबंधी रिकॉर्ड और रजिस्टर रखने में ज्यादा छूट की अनुशंसा की गई है। पहले तीन रजिस्टर रखने का प्रावधान था, जिसे घटाकर दो कर दिया गया है। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन के बाद, चतुराईपूर्ण ढ़ग से जब वे (फैक्ट्री मालिक) स्वयं को लघु उद्योग की श्रेणी में ला खड़ा करते है। तो इसका साफ मतलब ये है कि, उन्हें मनमर्जी से फैक्ट्री बन्द करने और श्रमिकों का छंटाई करने का अघोषित अधिकार मिल जाता है।
अब स्थिति ये बनती है कि, फैक्ट्री मालिक श्रम विभाग व शासन-प्रशासन से गठजोड़ करके, 60-70 मजदूरों को नियोजिता करने वाली कम्पनियाँ भी अपने आप को लघु उद्यम सिद्ध कर देती है। और कम्पनी रिकॉडों में मजदूरों की संख्या 10 से कम करके दिखाती है। इसके समानान्तरीय एक और नया रास्ते का सूत्रपात गत दशकों से हुआ है। मजदूरों को ठेके पर लेकर काम करवाना। इससे फैक्ट्री मालिकों को प्रत्यक्ष लाभ ये पहुँचता है कि, जिस करखाने में मजदूर ठेके पर काम पर रखे जाते है। उनकी गिनती कारखाने के मजदूर के रूप में नहीं की जाती।
किसी विवाद की स्थिति में फैक्ट्री मालिकों को, ये कहने में जरा भी झिझक नहीं होती, फलां मजदूर के प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं बनती, क्योंकि वो मेरे यहाँ ठेकेदार द्वारा काम पर रखा गया है। जवाबदारी है तो ठेकेदार की। जब वेतन संबंधी, दुर्घटना के मुआवजों के लेकर ठेकेदार का दायित्व आता है तो, वो रटे-रटाये लफ्ज़ों में जवाब देता है कि, मेरे और फैक्ट्री मालिक के बीच श्रमिक शक्ति उपलब्ध करवाने को लेकर, कुछ महीने या कुछ ही दिनों की कॉन्ट्रेक्ट हुआ है।
ऐसे में मुझे उस फैक्ट्री मालिक से इतना धन नहीं मिल पाता कि, मैं श्रमिक कल्याण, वेतन, दुर्घटना संबंधी मुआवजा जैसी चीजों के बारे में सोचूं या कुछ करूँ। इन दोनों रास्तों की मदद से फैक्ट्री मालिक स्वयं को कारखाना अधिनियम के तहत जरूरी दायित्वों से अलग कर लेता है। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन से मजदूरों के शोषण में भारी इजाफा होगा। इसकी कल्पना सहज ही लगाई जा सकती है।
फैक्ट्री एक्ट में एक और बदलाव है। स्पैड ओवर टाइम का यानि की मजदूरों को कारखाने में रोकने का समय। पहले ये समय 10:30 घण्टे था। पर विशेष परिस्थतियों में मुख्य कारखाना निरीक्षक (Chief Inspector Of Factories) की अनुमति के बाद इसे बारह घण्टे किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन के बाद फैक्ट्री मालिक, मजदूरों को अपनी मनमर्जी से बारह घण्टे से बढ़वाकर सोलह घण्टे करवा सकते है। पर इससे लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक (Chief Inspector Of Factories) की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
यदि इस संशोघन को बारीकी से देखा जाए तो, हम पाते है कि, फैक्ट्री एक-तिहाई माह में ओवर टाइम के घण्टों को 50 घण्टे से 100 घण्टे करने तथा बिजली की उपलब्धता के आधार पर साप्ताहिक अवकाश तय करने का अधिकार फैक्ट्री मालिकों को मिलेगा। यानि की जिस दिन उत्पादन के लिए विद्युत आपूर्ति रुकी तो उस दिन मजदूरों के लिए साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया जायेगा। पहले के प्रावधानों में एक ही औद्योगिक क्षेत्रों में एक ही दिन का साप्तहिक अवकाश उन क्षेत्रों के मजदूरों को मिलता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब एक ही औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अलग-अलग साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।
ऐसा करने के लिए फैक्ट्री मालिक को स्वतन्त्रता मिल जायेगी। इससे साफ तौर पर यहीं जाहिर होता है कि, ना सारे मजदूर एक दिन, एक साथ मिलेगें और नाही उनमें एकता और वर्गीय चेतना का उद्भव होगा। यानि की मजदूर अपने हितों की आव़ाज नहीं उठा पायेगें। और उद्योगपतियों को मजदूरों की तरफ से प्रतिरोध का सामना ना के बराबर झेलना पड़ेगा। पूंजीपति वर्ग महिलाओं को बेहद सस्ते श्रम का स्रोत, आज्ञापालक व श्रमशाक्ति की कीमत कम करने के उपकरण के बतौर देखता है। प्रस्तावित संशोधन होने के बाद, एक बड़ा बदलाव महिलाओं से रात की पाली में काम करवाने तथा उन्हें प्राइम मूवर सहित खतरनाक जगहों व मशीनों पर नियोजन करने में छूट मिल जायेगी।
पहले रात दस बजे से प्रातः छह बजे तक महिलाओं को कारखाने में नहीं रोका जा सकता था। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनायें बढ़ सकती है। अप्रेन्टिस एक्ट में संशोधन का प्रावधान रखा गया है। फैक्ट्रियों में अप्रेन्टिस रखना अनिवार्य कर दिया जायेगा। इसके साथ ही अप्रेन्टिस से किसी विवाद या उत्पीड़न की स्थिति में, कारखाना प्रबन्धन में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस संशोधन के बाद कारखाना प्रबन्धन को मनमानी संख्या में अप्रेन्टिसों को रखने में छूट मिल जायेगी। इससे फैक्ट्री मालिक को कम कीमत पर, कुशल श्रम का निर्बाध रूप से दोहन करने का अवसर मिलेगा।
अप्रेन्टिसों से उत्पीड़न के मामलों में कानूनी रक्षा कवच मिलने के बाद, पूंजीपति इन लोगों के प्रति गुलामी वाली परिस्थितियाँ बनाकर काम लेगा। अप्रेन्टिस अवधि पूरी हो जाने पर, इन अप्रेन्टिसों के सामने दो ही विकल्प बचते है। या तो वो बेरोजगारों की फौज में शामिल हो जाये या फिर किसी और पूंजीपति को सस्ती दर, अपने कुशल श्रम को उपलब्ध करवाये। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रिटर्न भरने तथा रजिस्टर रखने संबंधी छूट प्रदान करने वाले कानून के अन्तर्गत पहले 10-19 मजदूरों वाले उद्यम आते थे। पर अब इस अन्ध प्रस्तावित संशोधन के बाद मजदूरों की संख्या की सीमा बढ़ाकर 10-40 मजदूरों वाले उद्यमों तक कर दी गयी है।
उनके वेतन, हाजिरी संबंधी, दस्तावेज रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जायेगी है। ताकि पूंजीपति द्वारा श्रम कानूनों संबंधी उल्लंघनों से संबंधित कोई दस्तावेज ही ना रहे। अब कुछ सजावटी किस्म के श्रम कानून देखिये, जो हमारे देश निजामों द्वारा मजदूरों का कोढ़ खुजलाने का नाटक मात्र है। हर फैक्ट्री में शीतल व स्वच्छ जल की उपलब्धता को अनिवार्य करना। जिन औद्योगिक संस्थानों में 75 मजदूर काम करते है। उन्हें कैंटीन की व्यवस्था देना। पहले कैंटीन की सुविधा देने के लिए 250 मजदूरों वाले औद्योगिक संस्थान का होना जरूरी था। इस सुविधा के लिए मजदूरों की संख्या 250 से घटाकर 75 कर दिया गया है। सरकारें इन्हें प्रगतिशील और सकारात्मक कदम मानती है, ये एक हास्यापद बात है। महिलाओं को रात्रि पाली में सुरक्षित लाने व ले जाने की व्यवस्था करना।
बाल श्रम आरोपियों पर जुर्माने की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करना तथा सजा की अवधि 3 से 6 माह की जगह 6 माह से 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन मजदूर वर्ग अपने पूर्व अनुभवों से जानते है कि, इन कानूनों को कितने प्रभावी ढ़ग से लागू सकेगा। यदि इन कानूनों पर सूक्ष्म ढ़ग से दृष्टिपात किया जाये तो हम पाते है कि, ये सहज मानवाधिकारों की श्रेणी में आते है। विश्व की कोई भी विवेकशील प्रबुद्ध सरकार अपने श्रमिकों के लिए सहज उपलब्ध करवायेगी।
इसके लिए संशोधन, बिल, कानून बनाने जैसे जुमले मात्र चोंचले ही है। इन बुनियादी जरूरतों को देकर, हिन्दुस्तानी सियासतदां जमात खुद को मजदूरों का हमदर्द साबित करने में लगी हुई। जबकि इन सब चीजों के लिए किसी कानूनी प्रावधान की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सहज ही मिल जानी चाहिए।
इन श्रम सुधारों के बाद पहले से जो श्रम सुधार त्वरित कार्यवाही की सूची में है। उनमें कारखाना बन्द करने के लिए छूट सीमा को बढ़ाया गया है। सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 से श्रमिक करने, हड़ताल के दौरान समझौता वार्ता हेतु यूनियन की मान्यता शर्त 30 फीसदी मजदूरों की रजामन्दी। ऑटो परिचालन क्षेत्र को आवश्यक सेवा के अन्तर्गत लाकर, इसमें आवश्यक सेवा अधिनियम (ESMA) लागू कर हड़तालो को गैर-कानूनी बनाना।
यानि की रेलवे से जुड़े मजदूर संघ हड़ताल करेगें तो उसमें आवश्यक सेवा अधिनियम (ESMA) लागू नहीं होगा। जबकि रेलवे मजदूर संघ सरकारी मजदूर का संगठित संघ है। जिनके लिए तरह-तरह की सुविधायें और रियायतें उपलब्ध है। तुलनात्मक रूप से ऑटो वाले काफी पिछड़े है। जब वे अपनी जायज माँगो से साथ हड़ताल पर उतरते है तो एस्मा लगाकर, उनकी हड़तालों को कथित रूप से गैर-कानूनी घोषित कर दिया जायेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Dispute Act) के अध्याय 5(बी) को पूरी तरह से बदल दिया जायेगा।
अभी इस हिस्से में 100 ज्यादा मजदूरों वाले उद्यमों में, छंटनी, तालाबन्दी से पहले सरकार की अनुमति लेने का प्रावधान है। अन्य सुधारों में काम के घण्टे बढ़ाना, सलाना सवैतानिक छुट्टियों में कटौती, ट्रेड यूनियन के गठन और पंजीकरण के बाद भी, यूनियनों को कानूनी मान्यता व रक्षा हासिल करने की प्रकिया को जटिल बनाना। हड़ताल से पहले मतदान करवाना, तथा मौजूदा 14 दिन की पूर्व चेतावनी के समय को, छह माह करना। ताकि हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित किया जा सके। यदि आज लिए गये संस्थान प्रबन्धकों या फैक्ट्री मालिको के किसी निर्णय से मजदूर हताश और निराश है तो उन्हें हड़ताल करने के लिए, औद्योगिक संस्थान को छह माह की पूर्व चेतावनी देनी पड़ेगी। निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 6 महीने बाद होगा। तभी ये कानूनी माना जायेगा। अन्यथा गैर कानूनी कृत्य की श्रेणी में आयेगा।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) वास्तव में मजदूरों को पूरी तरह दासवत् स्थिति में रखने वाली श्रम जेले है। इनमें किसी भी प्रकार के श्रम कानून लागू नहीं होते है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों की रखवाली करने की जिम्मेदारी विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की है। यानि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए नियुक्त कर रखा है। भारत के तथाकथित पूंजीपति श्रम कानूनों को समाप्त कर ‘हायर एण्ड़ फायर’ वाली नीति लागू करवाना चाहते है।
भारतीय श्रम कानून पूंजीपतियों के पक्ष में, एक ओर ढ़ग से काम करता है। यदि श्रम कानूनों के तहत कोई मसला मेल-मिलाप, मध्यस्थता या न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा हो तो, ऐसे में हड़ताल, आंदोलन, गैर कानूनी होगें और दण्डनीय भी। पूंजीपति के लिए ये स्थिति अमोघ अस्त्र का काम करती है। जिसका इस्तेमाल कर वो विवाद को लम्बा खींचता है, और खींचता भी है। ऐसा सामान्य व्यवहार में देखने को मिलता है। इन विलम्बकारी हथकंडों के जाल में फंसकर मजदूर बुरी तरह थककर पस्त हो जाते है। भारत में तकरीबन 3 लाख औद्योगिक इकाइयां लकवाग्रस्त है, यानि बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है।
ये औद्योगिक इकाइयां देश की कुल औद्योगिक इकाइयों की करीब 8-9 फीसदी है। बेहतर ढ़ग से काम ना कर पाने का ठीकरा संस्थान के मालिक और पूंजीपति हड़तालों और यूनियनबाजी के सिर फोड़ते है। विगत दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन परिस्थितियों का आकलन करने के लिए, एक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। इस सर्वेक्षण से जो परिणाम निकल कर सामने आये, वो पूंजीपतियों के गाल पर करारा तमाचा है। परिणाम के अनुसार 65 फीसदी औद्योगिक इकाइयों का बेहतर ढ़ग से काम ना कर पाने का कारण संस्थागत प्रबन्धकीय नीतियां है। जबकि मात्र 3 फीसदी मजदूर व हड़ताले थी। इससे यहीं बात निकलती है कि, प्रबन्धकों में तमीज पैदा करने की बजाय, सरकारें, शासन-प्रशासन, व श्रम आयोग मजदूरों को ही घेरने की कोशिश करता है।
दमन चक्र केवल मजदूरों पर ही घूमता है। भारतीय श्रम आयोग की रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का कोई जिक्र नहीं है, यह उसके लिए छुट्टियों की श्रेणी में नहीं आता है। और ना उसके लिए मजदूरो के अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने के संघर्ष को कोई महत्तव है। आयोग बेधड़क होकर 9 घण्टे के कार्यदिवस की बात करता उछालता है। पिछले वर्ष में समाज के कई हिस्सों से ये मांग उठाई जाती रही है कि संविधान में संशोधन करके काम को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ला खड़ा किया जाये। देश की मजदूर यूनियनों ने भी श्रम आयोग से ये आस लगा रखी थी कि वो ये सिफारिश करेगा कि, काम के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी से निकाल, मौलिक अधिकार घोषित किया जाये। परन्तु ये आस, आस ही बनी रह गई।
श्रम आयोग की रिपोर्ट पैरा 6.109 में आयोग ठेका प्रथा को कम करने (एवं 1965 के कानून के अनुरूप समाप्ति) की वकालत करने की बजाय, काम का कोर और नॉन कोर श्रेणियों में विभाजन करता है। कोई भी उद्योग जो कि वर्ष भर चलना है, वहाँ पर काम के लचीलेपन व चुस्ती के नाम पर नॉन कोर गतिविधियों में ठेका प्रथा लागू करने का हिमायती कर रहा है। नॉन कोर गतिविधियाँ यानि कैंटीन व्यवस्था, देखरेख, साफ-सफाई। यानि की इन श्रेणियों में काम करने वाले लोग ठेका प्रथा के जुयें के नीचे दबे रहेगें। श्रम आयोग की रिपोर्ट पैरा 5.34 और 5.35 सीधे रखो और निकालो के बारे में कुछ नहीं कहता है। पर इसी बात का घुमा-फिराकर समर्थन जरूर करता है।
ये कहता है कि किसी भी इकाई में ठेका प्रथा को एकदम से लागू नहीं किया जाना चाहिए और लागू करने से पूर्व कानूनी पचड़ों से निपटे की तैयारियां (जिसे आयोग पूर्व तैयारियाँ कहता है) कर लेनी चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाये तो, आयोग की निगाह में ये उचित ही होगा। लेकिन ठेकाकरण की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए, ताकि इसकी भनक से कानून व्यवस्था को कोई खतरा ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (Industrial dispute Act-1947) के अनुच्छेद 9-ए का लेना-देना उस नोटिस से है। जो नोटिस नियोक्ता (Employer) को तब देना चाहिए, जब वह मजदूर के काम की स्थितियों में कोई परिवर्तन करना चाहता है। अनुच्छेद 9-ए कहता है कि, यह नोटिस कार्य में परिवर्तन से 21 दिन पहले दिया जाना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई IDA1947 की चौथी अनुसूची के बिन्दु 10 का लेना देना मशीनरी/तकनीकी/कार्य पद्धति के उन परिवर्तनों से है। जिससे छंटनी की स्थितियाँ पैदा होती है, IDA-1947 की चौथी अनुसूची के बिन्दु 11 का लेना देना किसी शिफ्ट/विभाग/प्रक्रिया कार्य में लगाये गये मजदूरों की संख्या में वृद्धि और कमी से है। जो नियोक्ता के नियन्त्रण में है, पूंजीपतियों के संगठन, मजदूरो के कार्यों की स्थितियों में मनचाहे परिवर्तन के अधिकार चाहते है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 के अनुच्छेद 33 मालिको को, ऐसे किसी भी मजदूर के कार्य की स्थितियों में परिवर्तन करने से रोकता है। जिसका मामला लेबर डिपार्टमैन्ट या कचहरी में हो। श्रम आयोग की रिपोर्ट के पैरा 6.88 में गहन विचार-विमर्श के बाद आयोग निम्न सिफारिशें करता है
- किसी भी बड़े आकार के संस्थान में ले-ऑफ या छंटनी के पूर्व किसी भी प्रकार की सरकारी अनुमति की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
- छंटनी करने से दो महीने पहले मालिक केवल मजदूर को नोटिस देगा। यदि वह पूर्व नोटिस ना देना, चाहे तो नोटिस के एवज में, दो माह का वेतन दे सकता है।
- जिन इकाइयों में 300 से ज्यादा मजदूर काम करते है, वहाँ ले-ऑफ के, एक माह बाद सरकारी स्वीकृति लेनी होगी।
औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 के अध्याय 5-बी को केवल फैक्ट्रियों, खदानों, बगानों पर ही लागू ना किये जाये। बल्कि अन्य संस्थानों को भी इसके अन्तर्गत माना जायेगा, लेकिन इनके तहत उन्हीं संस्थानों को माना जायेगा, जहाँ 300 से अधिक मजदूर साल भर काम करते है। 100 मजदूरों वाली पुरानी मियाद को ऊपर उठाकर 300 तक लाया जाये। जिन औद्योगिक संस्थानों में वर्ष भर 300 से कम मजदूर काम करते है। उन संस्थानों को को बिना किसी पूर्व सरकारी अनुमति के बन्द किया जा सकेगा। ऐसे संस्थान जहाँ 300 से अधिक स्थायी मजदूर साल भर काम करते है।
यदि वे संस्थान मालिक, अपनी औद्योगिक इकाइयों को बन्द करना चाहे, तो उन्हें ऐसा करने से तीन माह पूर्व संबंधित सरकार को आवेदन देना होगा। यदि आवेदन देने के 60 दिनों बाद संबंधित सरकार आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो, संवैधानिक रूप से ये माना जायेगा कि, औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने की सरकारी मान्यता मिल चुकी है। इस कानून का मतलब पूंजीपति की चिट और पट दोनों है। यदि ये अनुशंसायें लागू हो जाती है तो, उद्योगपति जब चाहेगें तब ले-ऑफ, छंटनी और बन्दी करने की मनमानियां करने लगेगें। बस 300 से ज्यादा मजदूरों वाले संस्थानों के मालिकों को सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी घूस देकर अपनी औद्योगिक इकाइ को बन्द करने के आवेदन को 60 दिनों के लिए रूकवाना होगा। आगे का काम खुद ही आसान हो जायेगा।
आज IDA के अध्याय 5-बी के हटाने के लिए सिफारिशें की जा रही है। पूंजीपति मजदूर से निरीक्षण करवाने के अधिकार को छीनना चाहता है, और साफतौर पर ‘रखो और निकालो’ का अधिकार पाना चाहता है। कहीं बोल्शेविको की तरह मजदूर भारत में तख्ता पलट ना कर दे। इसलिए ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों ने 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट (Trade Union Act-1926) बनाया। इस कानून की मुख्य बात यूनियनों के पंजीकरण से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक काल में, पंजीकृत और गैर-पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का कोई बंटवारा नहीं था। परन्तु इस अधिनियम के कारण अंग्रेजो ने गैर-पंजीकृत यूनियनों को गैर-कानूनी दर्जा देने की कोशिश की। उस समय इस कार्रवाई का जमकर विरोध हुआ। तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि, मजदूरों का कोई संगठन आसानी से पंजीकरण करवाकर प्राथमिक स्तर पर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता था। पर समकालीन परिस्थतियों में ऐसा नहीं है, आज श्रम कानून इस प्रक्रिया को श्रम साध्य और दुष्कर बनाने में उतारू है। ये संस्तुति देता है कि, किसी श्रमिक समूह का ट्रेड यूनियन के बतौर तब तक पंजीकरण न किया जाये, जब तक उस संस्थान/फैक्ट्री के 10 प्रतिशत मजदूर (या 100 श्रमिकों का, जो भी कम हो) का समर्थन हासिल ना हो।
सहज अन्दाजा लगाया जा सकता है, ट्रेड यूनियनों की प्रक्रिया दुष्कर होगी तो, मजदूरों को इसका गठन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनकी लाचारगी की फेहरिस्त में, इजाफा हो जायेगा। अपनी जायज माँगों को मनवाने में वे असहाय महसूस करेंगे। श्रम आयोग का मानना है कि, ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण हो जाने भर से, मालिक आपको मजदूर के प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता नहीं देगा। श्रम आयोग के पैरा 6.66 में आयोग फरमाता है कि, मान्यता पाने के लिए किसी भी ट्रेड यूनियन को कम से कम औद्योगिक संस्थान या फैक्ट्री मे काम करने वाले 25 फीसदी मजदूरों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। केवल ऐसी यूनियनें जिन्हें 25 फीसदी से अधिक श्रमिकों का समर्थन प्राप्त है। प्रबन्धन से बात करने के लिए बाध्य होगी। श्रम आयोग 6.76 कहता है कि, ट्रेड यूनियनों की मान्यता रोज-रोज नहीं बांटी जायेगी। मान्यता देने की प्रक्रिया चार वर्षों में एक बार की जायेगी। एक बार तय हो जाने के बाद, जब तक चार वर्ष नहीं बीत जाते तब तक किसी यूनियनों/फेडरेशन/केन्द्र को यह अधिकार नहीं होगा कि, वह मान्यता के लिए दावा पेश करे। मजदूर के प्रतिनिधि के तौर पर खुद को पेश कर सके।
अर्थात् प्रबन्धन की नीतियों या मालिक के किसी फैसले से श्रमिकों को कोई दिक्कत है तो उन्हें मजदूर यूनियन का मान्यता के साथ गठन कर, अपनी बात रखने के लिए चार वर्ष का इन्तजार करना पड़ेगा। ये बात किसी मूर्ख के लिए भी हास्य का विषय हो सकती है। इन सारी कवायदो से परिणाम निकलेगा कि, मजदूर हितों के लिए लड़ने वाले सच्चे ईमानदार लोग आगे ना आ सके। ढेर सारी बाधाओं को खड़ा करके, पहले तो ट्रेड यूनियनों के गठन को रोका जाता है, यदि औपचरिकता पूरी करके श्रमिक वर्ग ट्रेड यूनियन बना भी लेता है तो, मजदूर के प्रतिनिधि के तौर पर प्रबन्धन या मालिको की तरफ से मान्यता ही ना मिले, ऐसा प्रबन्ध किया जाता है।
हर जगह ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई, हड़ताल को मान्यता प्राप्त करने के लिए गुप्त मतदान के प्रक्रिया अपनाई जाती है। हड़ताल करने कके लिए 51 प्रतिशत मजदूरों का समर्थन हड़ताल के पक्ष हासिल करना आवश्यक है। बिना 51 फीसदी समर्थन के, बुलाई गई हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया जायेगा, और ऐसी हड़ताल भाग लेने वाले श्रमिकों को दण्ड़ का भागी होना पड़ेगा।
दण्ड़ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, गैर कानूनी हड़ताल के प्रत्येक दिन के लिए, मजदूरों को तीन दिनो का वेतन देना होगा। इसके साथ आयोग अपनी निष्पक्षता की नंगी नुमाईश करते हुए आयोग ऐलान करता है कि, लॉक आउट की स्थिति में मालिक को भी इसी दर से दण्ड़ देना होगा। आयोग हड़ताल बुलाने के लिए 51 फीसदी मजदूरों की रजामन्दी की मांग तब कर रहा है, जब वो मालिको को ‘रखो और निकलो’ का अधिकार दे चुका है। यदि हड़ताल गैर कानूनी हुई तो आर्थिक दण्ड़ के साथ आयोग ये भी कहता है कि, उक्त यूनियन (जिन्होनें हड़ताल का आवाह्न किया था) की मान्यता का निरस्तीकरण कर दिया जाये।
एक पंजीकरण निरस्त होने पर हड़ताल का नेतृत्व करने वाली यूनियन को अगले 2-3 वर्षों के लिए निषिद्ध कर दिया जायेगा। यानि हड़ताल का नेतृत्व करने वाली यूनियन को 2-3 वर्षों का वनवास। किन्तु यह आयोग अपनी निष्पक्षता को दोहराने में असर्मथ रहा है। आयोग यह सिफारिश नहीं कर सका कि, जो मालिक गैर-कानूनी तरीके से लॉक आउट करता है। उसकी फैक्ट्री का भी 2-3 वर्षों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ट्रेड यूनियनों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आयोग को मन्जूर नहीं है। मसलन् यदि ट्रेड यूनियन के अल्प शिक्षित मजदूर अपनी यूनियन को मजबूत करने व सलाहकार के तौर किसी प्रबुद्ध व्यक्ति जो कि श्रम कानूनों विशेषज्ञ है। को अपने साथ जोड़ना चाहते है, इसके लिए आयोग ने सीमायें बांध दी है। इससे जाहिर होता है, आयोग की नज़र में बाहरी व्यक्ति नकारात्मक है।
इनकी गिनती यूनियन की कार्यकारिणी एक तिहाई या पाँच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयोग ऐसा भी साफ करता है कि, कोई व्यक्ति जो कभी संस्थान में काम करता था। और अब सेवानिवृत है या छंटनी का शिकार है, को बाहरी व्यक्ति ही माना जायेगा। श्रम आयोग के पैरा 6.51 में आयोग सुझाव देता है कि, ट्रेड यूनियन एक्ट-1926 के तहत नियोक्ताओं (Employer) के संगठनों का गठन भी कतई जायज नहीं है। आयोग कहता है कि, इस प्रथा को आदरपूर्वक जारी रखा जाये। यानि आगे भी नियोक्ताओं के संगठनों (Employer Association) को ट्रेड यूनियनों का दर्जा मिलता रहेगा। और इस हैसियत से वे जगह-जगह संयुक्त समन्वय समितियों अथवा अन्य मजदूरों के मन्चों पर घुसपैठ करेगें।
आयोग यूनियन को कारखाना/फैक्ट्री/औद्योगिक संस्थान के प्रबन्धन में हिस्सेदारी जैसे अहम् मुद्दे के लिए सीधे-सीधे घोषणा करता है, इसे प्रबन्धकों या यूनियनों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए बाकयदा अलग से कानून बनाना चाहिए। आयोग ट्रेड यूनियनों से शत्रुता नहीं रखता है, वह इन्हें पूंजीपतियों के हितो के लिए हर तरह से उपयोगी बनाना चाहता है, आयोग जिस चीज से दुश्मनी रखता है, वह है ट्रेड यूनियन में घुसपैठ करने वाली क्रान्ति चेतना से।
भारत के पूंजीपति में से कई ये मानते है कि, औद्योगिक संबंधों के नियन्त्रण राजसत्ता की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक संबंध विशुद्ध द्विपक्षीयता और मांग-आपूर्ति के नियम द्वारा नियन्त्रित होने चाहिए। आयोग की रिपोर्ट पैरा 1.25 में ऐसे लोगों का पक्ष है, जो कि ये फरमाते है, राजसत्ता की भूमिका निजी सम्पत्ति की रक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने तक ही सीमित रखी जाये। मजदूर वर्ग उन लोगों की इस मांग को शिरोधार्य करता है, यदि वे लोग इसे तार्किक परिणति तक पहुँच दे। अर्थात् जीवन के हर क्षेत्र में इसे यानि की राजसत्ता की भूमिका को खत्म करने के लिए तैयार हो जाये।
औद्योगिक संबंधों का नियन्त्रण ही क्यों। राजसत्ता को निजी सम्पत्ति व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाये। हर मसले को द्विपक्षीयता से ही तय होने दिया जाये, कैसा रहेगा ? भांति-भांति की मुकदमेबाजी और लम्बी थकाऊ दीर्घकालिक न्यायप्रक्रिया के चलते औद्योगिक विवादों का कोई निपटारा नहीं हो पाता है। जिससे आहत मजदूर पक्ष के साथ इन्साफ नहीं हो पाता है। भोपाल गैस काण्ड़ इस तथ्य का रक्तरंजित उदाहरण है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुच्छेद 11-ए को बनाये रखा जाए। पर न्यायालयों की उन शाक्तियों का स्थगन कर दिया गया है। जिनमें वे दोषी पाये जाने के बाद भी मजदूर को नौकरी लगवा सके।
इस अनुच्छेद के अन्तर्गत पुरानी बात यह थी कि, हिंसा तोड़-फोड़, अगजनी, चोरी इत्यादि के आरोपों में मालिक मजदूर को नौकरी से बेदखल कर देता है। तब भी अदालतों को ये हक था कि, वो मजदूर को दुबारा नौकरी पर लगवा सके। ऐसा करने के पीछे अदालतों का यह तर्क था कि, सजा गुनाह के अनुसार होनी चाहिए। छोटी गलती करने के लिए नौकरी से निकलने जैसी गंभीर सजा नहीं दी जा सकती है। पर आयोग इस सिफारिश का खारिज करके न्यायालय से ये अधिकार छीनना चाहता है। और हाकिमों के हाथ में मजदूरों का शोषण करने के लिए। चाबुक देना चाहता है। मजदूर के पेट पर लात मारे जाने को जायज ठहराते हुए। 11-ए में परिवर्तन के लिए झण्ड़ा बुलन्द करना चाहता है।श्रम आयोग का कहना है कि, अनुच्छेद 2-ए को भी बदला जाये। यदि किसी मजदूर का (या मजदूरों के समूह का) मालिक से किसी बात पर विवाद हो जाये। और मालिक उसे (उन्हें) नौकरी से बर्खास्त कर दे, तो ये निजी मामलों की श्रेणी में आयेगा।
आयोग इस मसले पर अपनी राय कायम करते हुए, तहरीर देता है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन ऐसे मामलों में सुलह, मध्यस्थ निर्णय इत्यादि में श्रमिकों की पैरवी करती है। परन्तु उसे इन मामलों को औद्योगिक विवाद बनाने का अधिकार नहीं होगा। लबोलुआब ये है, यदि मालिक किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दे। तो उस मजदूर की ट्रेड यूनियन या अन्य यूनियनें इस मामलें पर हड़ताल या आंदोलन नहीं कर सकती है। ऐसी दशा में वे रक्षात्मक कार्रवाई करे तो वह गैरकानूनी होगी, अर्थात् मालिक अगर रोज एक-एक करके मजदूरों को निकलता रहे। तब भी यूनियन को औद्योगिक शान्ति की पवित्रता को बनाये रखना होगा। घुमा फिराकर आयोग मालिको को ‘रखो निकालो के अधिकार’ से लैस कर रहा है। श्रम आयोग 6.99 में तहरीर देता है कि, सुलह या लोक अदालत में किसी भी पक्ष को पेशेवर वकील रखने का अधिकार नहीं होगा। न मालिक के पक्ष को और ना ही श्रमिकों के पक्ष को। इससे ये सार्थकता प्रामणित होती है, ऐसा होने पर श्रमिक संबंधी मामलों का निपटारा जल्दी जल्दी होगा। अन्यथा मामले लम्बे-लम्बे खिंचेगें। ऐसा करके आयोग मालिक के पक्ष में न्याय को और सुलभ करवाता है।
व्यावहारिक जीवन में देखने को मिलता है कि, मालिक और मालिक प्रतिनिधि पढ़े लिखे लोग होते है, कानूनी जानकारी और न्याय व्यवस्था के छल-छिद्रों से भली-भांति परिचित होते है। और दूसरी आँखों में न्याय की गुहार लिये उनके प्रतिपक्षी मजदूर लोग कम दुनियादार कम वाचाल और कम पढ़े लिखे लोग होते है। मालिकों और उनके प्रतिनिधियों का पेशा ही लेबर मैनेजमेंट का होता है। ऐसे चतुर, पेशेवर लोगों का, एक नौसिखिया मजदूर यूनियन, एक गैर पेशेवर मजदूर कैसे कर सकता है। ऐसे मामलों में मजदूरों को बराबरी का दर्जा देने के लिए, मजदूरों को वकील खड़ा करने की छूट देनी चाहिए, और मालिकों को ये पाबन्दी होनी चाहिए कि, वे कोई पेशेवर वकील न खड़ा कर सके। दोनों तरफ से पेशेवर वकील खड़ा करने की छूट से भी बराबरी हासिल नहीं की जा सकती है। क्योंकि पैसे और सम्पर्क के बल पर मालिक ज्यादा मंहगा और सक्षम वकील का इन्तजाम कर लेते है।
श्रम मामलों में न्यायिक ढांचे के पुर्नगठन में आयोग का प्रस्ताव तीन स्तरों प्रान्त, केन्द्र एवं राष्ट्रीय स्तर श्रम संबंधों के आयोग को स्थायी निकाय के बतौर गठित करने की सिफारिश है। ‘श्रम संबंधों के आयोग’ ऐसे निकाय होगें जो श्रम कानूनों की परिधि में आने वाले हर मामलें पर अन्तिम सुनवाई के मन्च होगें। इनमें मामले के उठने या फैसला हो जाने के बाद उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं होगा।
आयोग ने यह निर्धारित किया है कि, ऐसे संस्थान जहाँ 20 से कम लोग काम करते है, को ही लघु उद्यम (Small Enterprises) माना जायेगा। आयोग ये साफ करता है कि लघु उद्योग जिस कानून के तहत लागू किये जाये। वे आम कानून का हिस्सा नहीं होगा। इनके के लिए विशिष्ट कानून बनाया जायेगा। जिसे आम कानून के विशिष्ट अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आयोग दो एक बातें साफ करता है। लेकिन वे महत्त्वपूर्ण हैं। पहली यह है कि इनके मालिक सरकारी निरीक्षण के दायरे से बाहर होगें। उन्हें अपने उद्यम को स्वयं प्रमाणपत्र दे देना होगा।
उनके कारखानों/संस्थानों में सरकारी अधिकारी तभी निरीक्षण करेंगे जब वे सरकार के पास प्रमाणपत्र भी ना जमा करे या फिर उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्जा हो। दूसरी यह कि मालिक परेशानियां गिनवाकर ले-ऑफ ले कर सकता है, बशर्ते वो ले-ऑफ के दौरान मजदूरों को मुआवजे के रूप में उनके वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करे। और यदि ले-ऑफ 45 दिन से अधिक हो तो मजदूरों की नौकरियां खत्म करने के लिए मालिक कानूनी रूप से अधिकृत होगा। तीसरी यह कि लघु उद्यमों के लिए जो कानून लिखा जायेगा उसमें फैक्ट्री अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, औद्योगिक रोजगार अधिनियम-1946, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम-1936, बोनस भुगतान अधिनियम-1965, कर्मचारी प्रोविडेण्ट फंड एवं विविध मद अधिनियम-1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948, मातृत्व लाभ अधिनियम-1961, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, समान वेतन अधिनियम-1976, ठेकेदार श्रमिक अधिनियम-1972 इत्यादि धारायें लागू नहीं की जायेगी।
वह कानून अत्यन्त सरल और छोटा होगा, हालांकि सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, बोनस इत्यादि का ध्यान कानून लिखते वक्त रखा जायेगा। श्रम आयोग की भाषा और टिप्पणियों से साफ है कि उसकी संवेदनायें इन लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के प्रति नहीं इनके मालिकों की कमजोर हालत के प्रति है। यह सारी राहत मालिकों को है। श्रमिकों को नहीं। लघु उद्योग काम करने वाले श्रमिकों को आयोग कुछ नहीं दे रहा है। उन्हें जो नाममात्र का कागजी संरक्षण प्राप्त था, वह भी आयोग छीन रहा है। हालांकि मजदूरों की सबसे ज्यादा दुर्दशा ऐसी ही इकाइयों में होती है। इन इकाइयों में मजदूर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर काम करते है। काम की स्थितियां भी बहुत बुरी होती है, मजदूरों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। इन सबके बावजूद आयोग सरकारी निरीक्षण प्रणाली खत्म करके, स्व प्रमाण पत्र प्रणाली को स्थापित कर रहा है। ऐसे में यदि मालिक कहे वो अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दे रहा है, तो सरकार मानती रहेगी कि वो अपने मजदूरों को न्यूनतम वेतन दे रहा है।
भले वो ना दे रहा हो। यदि मालिक कह दे कि वो ओवर टाइम के लिए दुगुने पैसे देता है। तो सरकार मानती रहेगी ऐसा हो ही रहा होगा। अब वह कार्यस्थल पर निरीक्षण की फर्ज अदायगी करने तब-तक नहीं जायेगी। जब तक कि उसके पास मजदूर इकट्ठे होकर औपचारिक शिकायत ही लेकर ना पहुँच जाये और तब भी सरकार मजदूरों की नौकरियों को बचाने की गारण्टी नहीं लेगी। उपरोक्त लेख का सारगर्भित निष्कर्ष यह है कि, नियमों और कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में ज्यादा झुका दिया गया है। दूसरा यह कि, श्रमिकों के लिए बने न्यायिक ढांचे में पूंजीपतियों के प्रतिनिधियों-अर्थशास्त्रियों ट्रेड यूनियन नौकरशाहों, नियोजकों की संस्थाओं के सदस्यों, भारतीय प्रशासनिक सेवा आधिकारियों आदि को घुसेड़ दिया गया है।
अर्थात् न्यायिक ढांचे के नाममात्र की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई है। ऐसे हालात में औद्योगिक विवादों का निपटारा फटा-फट पूंजीपतियों के हक में होता चला जायेगा। यदि तेजी ही लानी है और पूंजीपतियों की ही तरफदारी करनी है तो इससे बेहतर (और कहीं कम खर्चीला) होगा कि चार-पाँच कानून भी क्यों लिखे जाये। एक ही कानून बनाया जाये और वह भी एक ही वाक्य का ‘औद्योगिक विवादों में पूंजीपति हमेशा सही होता है’ आगे ढांचे के सरलीकरण के लिए पुलिस के थानेदारों को उक्त कानून के तहत फैसले सुनाने के लिए अधिकृत कर दिया जाये, बस। ऐसे में कुछ सवाल उभरकर आते है-
- बेहतर और प्रभावी श्रम कानून क्या विकास विरोधी अवधारणा है ?
- संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में क्या अन्तर होता है ?
- संगठित क्षेत्र में सक्रिय मजदूर यूनियनों की असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति, किस स्तर तक सह्रदयता और आत्मीयता होती है ?
- वर्तमान समय में, ट्रेड यूनियनों में वो पैनापन और सशक्तता क्यूँ नहीं दिखाई देती है, जो कि 70-80 के दशक में हुआ करती थी ?
- छोटी और गैर-पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले असंगठित श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ, कैसे पहुँचाया जाये ?
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम कानूनों के प्रति किस प्रकार जागरूक किया जाये एवं उनकी दयनीय दशा का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है ?
- देश के कुल कार्यबल का 93 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत का योगदान देता है, ऐसे में सरकारें इस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यापक और प्रभावी श्रम कानून बनाने में क्यों विवश दिखाई पड़ती है ?
- हमारे देश में उद्योग संगठित है, पर इनमें काम करने वाले मजदूर असंगठित हैं ऐसा क्यूँ ?
(सन्दर्भः- रियल स्टेट उद्योग संगठित तौर पर फल-फूल रहा है, परन्तु इनमें कन्सट्रक्शन का काम करने वाले श्रमिक असंगठित क्षेत्र के मजदूर के तौर पर काम करने के लिए अभिशप्त है।)