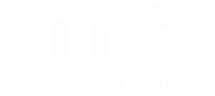कितनी घृणा है हमारे अपने समाज में। जो हमक़दम, हमराह साथ मिलकर संघ-जनित घृणा और असहिष्णुता को कोसते थे, आज वही समझाने लगे कि मृत्यु के बाद हिटलर-मुसोलिनी के साथ क्या किया गया था? उनकी ‘दलील’ इस बात पर कि मैंने सुझाया कि क्यों न किसी अप्रिय की मृत्यु की घड़ी में भी हम ज़रा बेहतर आचरण बरतें।
कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं थोड़ा हिटलर-मुसोलिनी को पहचानता हूँ और गोलवलकर, सावरकर, गोडसे, मोदी की जमात को भी जानता हूँ; मुझे आलोक मेहता, रजत शर्मा, स्वपन दासगुप्ता, सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, रोहित सरदाना (Rohit Sardana) आदि के काम के बारे में भी पता है। हज़ार बार लिखा होगा। अब भी लिखता हूँ और लिखूँगा। लेकिन घड़ी भर को, जब सामने से मृतक का शव गुज़र रहा हो, कोसना कुत्सित (Sickening) क़िस्म की अधीरता है। “मूल्यांकन” की दुहाई न दें। वह बहुत भारी शब्द है। उसका भी वक़्त होता है। और हर शख़्स मूल्यांकन की ऊर्जा लगाने के क़ाबिल भी नहीं होता।
कुछ लोग मंटो को बीच में ले आए हैं, जिन्होंने कहा था कि “मैं ऐसे समाज पर हज़ार लानत भेजता हूं, जहां उसूल हो कि मरने के बाद हर शख़्स के किरदार को लॉन्ड्री में भेज दिया जाए जहां से वो धुल-धुलाकर आए’। मंटो ने सही कहा। मरने के बाद समाज मरने वाले के चरित्र को संवारने का काम क्यों करे? लेकिन, “मरने के बाद” को “मरने की घड़ी” पढ़ लेना नादानी होगी। मूल्यांकन (Evaluation) फौरी काम नहीं होता। उसका समय आता है। तब बुरे को बग़ैर किसी लाग-लपेट बुरा ही कहना चाहिए। मगर, जैसा कि ऊपर कहा, हम ख़याल रखें हर शख़्स मूल्यांकन के क़ाबिल नहीं होता।
मेरा अब भी यही कहना है कि सामने महामारी के शिकार हुए किसी पत्रकार (या किसी अन्य) का शव गुज़र हो, तब कम-से-कम इतनी संवेदना हममें रहनी चाहिए कि उस घड़ी — घड़ी भर को सही — मृत्यु से आहत घर-परिवार, बेसाया हुए मासूम बच्चों और निर्दोष साथियों आदि के बारे में सोच सकें।
अर्थी उठते वक़्त जो मंटो का नाम लेकर किसी की “धुलाई” का आह्वान करें, वे न मंटो को समझते है, न मानवीय आचरण को।
साभार- ओम थानवी (वरिष्ठ पत्रकार)