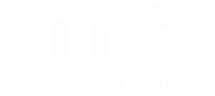इधर फिर से यरुशलम में इजराइल और फलस्तीन के बीच टकराव जारी है। वो एक दूसरी कहानी है। लेकिन इस्लामिक मनोविज्ञान (Islamic Psychology) पर पैनी नज़र रखने के कारण मैं देख रहा हूं कि लगभग सभी प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवी, कलाकार, खिलाड़ी इसमें फलस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठाए हैं और हैशटैग वगैरा के ज़रिए अंतराष्ट्रीय समुदाय और लिबरल्स (International Community and Liberals) पर सहयोग के लिये दबाव बनाए हुए हैं। मुसलमानों की राजनैतिक चेतना चकित करती है। कभी कभी लगता है इस्लाम एक रिलीजन या फलसफा या चेतना की धारा नहीं बल्कि एक राजनैतिक आंदोलन है जिसका मक़सद अपना प्रसार, वर्चस्व और अपने पक्ष में नरेटिव का निर्माण है।
पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर एकमत हैं कि कश्मीरी, रोहिंग्या, उईघुर, फलस्तीनी लोगों पर जुल्म हो रहा है लेकिन कुर्दों, यजीदियों, बलूचों, आर्मेनियाई कौम, शिया और अहमदियों पर हो रहे ज़ुल्म के लिए कोई आवाज़ उनकी बरामद नहीं होती। इतिहास में इस्लाम ने जितने ज़ुल्म किए, कत्ल किए, ख़ून बहाए, मुल्कों पर कब्ज़ा किया, मुल्कों को तोड़ा और हर जगह अपने मज़हब को फैलाने, मौजूदा कल्चर और तौर तरीके से खुद को अलग रखने और अलगाव और टकराव पैदा करने की कोशिश की, इस पर भी मुझको कोई बयान नहीं मिलता। फलस्तीन प्रश्न पर या वैसे किसी भी संघर्ष पर मुसलमानों से एक वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और ईमानदार राय की उम्मीद करना ही बेकार है। यहूदियों से इनको इस बात के लिए नफ़रत है कि ये हमारे मुल्क में घुस आए और काबिज़ हो गए, जबकि इस्लाम के प्रसार का पूरा इतिहास ही दूसरे मुल्कों में जाकर वहां फैल जाने का है, इसकी कोई व्याख्या मुस्लिमों के यहां नहीं मिलती।
फलस्तीन संकट के बारे में सुनकर मुझको कुर्दों की याद आई जिनकी कोई बात ही नहीं करता है। कुर्द एक ऐसी दु:खियारी और कमनसीब क़ौम है, जिसका अपना कोई मुल्क नहीं। आज की दुनिया में अगर किसी नस्ल के पास अपना स्वयं का कोई राष्ट्र ना हो तो उसे कैसी अमानवीय परिस्थितियों में जीना पड़ता है, कुर्दिश लोग इसकी मिसाल हैं। ये लोग पश्चिम-एशिया में मुख्यतया ईरान, इराक़, तुर्की और सीरिया में फैले हैं। इनकी तादाद साढ़े चार करोड़ के आसपास है, लेकिन अपना कोई देश नहीं होने के कारण ये उपरोक्त मुल्कों में अल्पसंख्यकों की तरह रहते हैं और अनेक प्रकार के अत्याचारों और मानवाधिकार-हनन (Human rights abuses) का शिकार होते हैं।
कहने को तो एक कुर्दिस्तान-रीजन है, लेकिन उसकी कोई सम्प्रभुता नहीं है। कुर्दों की अपनी एक कुर्दिश ज़बान है, अपनी पृथक सांस्कृतिक परम्पराएं हैं, किंतु उनको अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है। कुर्दों में सुन्नी मत की शफ़ी धारा के लोग हैं तो शिया और अलेविक मत के भी लोग हैं। इनमें से कुछ पारसी और ईसाई मत का भी पालन करते हैँ। इराक़ और ईरान दोनों में ही कुर्दिस्तान नाम के इलाक़े हैं, लेकिन उन्हें स्वायत्तता नहीं है।
सीरियाई युद्ध की एक उपकथा कुर्दों का प्रसार भी था। कुर्द राष्ट्रवाद इधर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, किंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उसकी चिंता नहीं है। कुर्द लोग अपना स्वयं का राष्ट्र चाहते हैं, किंतु अगर ऐसा होता है तो इराक़, सीरिया और तुर्की को अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ेगा, और ये मुल्क इसके लिए तैयार नहीं हैं। अपने मुल्क को तोड़कर उसका एक हिस्सा दूसरी कौम को दे देना सबके लिए इतना सहज नहीं होता। सभी मुल्कों का नाम हिंदुस्तान नहीं होता।
पश्चिम एशिया के दुर्भागे पहाड़ी इलाक़ों में आज़ाद-कुर्दिस्तान के बाग़ यहां-वहां खिले हैं, जिनसे किसी को हमदर्दी नहीं है।
1980 के दशक में ईरान-इराक़ जंग के दौरान सद्दाम हुसैन के हुक्म पर अनफ़ाल में कोई एक लाख 82 हज़ार कुर्दों का क़त्ल कर दिया गया था। यह नरसंहार इतना भीषण था कि इसे आधुनिक युग के सबसे भयावह हत्याकांडों में से एक माना जाता है। किंतु केवल चार ही राष्ट्रों (नॉर्वे, स्वीडन, यूके और दक्षिण कोरिया) ने इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी है। इसकी स्मृति को जगाए रखने के लिए कुर्दिश डायस्पोरा, जो विशेषकर तुर्की और जर्मनी में फैला हुआ है, 14 अप्रैल को अल-अनफ़ाल दिवस मनाता है।
कुछ ऐसी ही कहानी यज़ीदियों की भी है, जिनका बीते दशक में आईएसआईएस ने क़त्लेआम किया था। सिंजार और मोसुल के जेनोसोइड कुख्यात हैं। यज़ीदियों का भी अपना कोई देश नहीं है। उस्मानी साम्राज्य के तहत आर्मेनियाइयों का भी योजनापूर्वक नरसंहार किया गया था और पहले विश्व युद्ध के दौरान कोई डेढ़ करोड़ आर्मेनियाई मारे गए थे। शुक्र है कि आर्मेनिया अपना स्वयं का एक राष्ट्र प्राप्त करने में सफल रहा और 1918 में गठित फ़र्स्ट रिपब्लिक के बाद 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बना। येरेवान उसकी राजधानी है। आर्मेनिया की 98.1 बहुसंख्य आबादी आर्मेनियाइयों की है।
हम एक बहु-सांस्कृतिक दुनिया का सपना अवश्य देखते हैं किंतु यह भी सच है कि अगर किसी नस्ल का अपना कोई राष्ट्र न हो तो उसके लोग दुनिया में बंजारों की भांति भटकते रहेंगे और किसी को उनकी परवाह नहीं होगी।
मैं समझ नहीं पाता कि कश्मीरियों, रोहिंग्याओं और फ़लस्तीनियों के मानवाधिकार कुर्दों, यज़ीदियों, बलूचों और आर्मेनियाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इन दूसरे लोगों के बारे में बातें करता बरामद नहीं होता। स्वयं भारत में इनको लेकर कभी आंदोलन नहीं होते, गाज़ा-पट्टी को लेकर तो बहुत होते हैं। एक आश्चर्य यह भी है कि भारत का बहुसंख्य समुदाय वंचित-पीड़ित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए उमड़ आता है, किंतु ये वंचित-पीड़ित वर्ग कभी दुनिया के दूसरे वंचितों-पीड़ितों के हक़ की बात नहीं करते। यह ख़ुदगर्ज़ी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है कि आप हमेशा अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और इसमें दूसरों की मदद पाकर मुतमईन भी हों, लेकिन आप ख़ुद कभी औरों के हक़ की बात ना करें। और आपका नज़रिया हमेशा आपकी नाक से आगे देखने और सोचने में नाकाम रहे! इतना ही नहीं, आप इस ख़ुदगर्ज़ी और मौक़ापरस्ती को इंक़लाब भी कहें!
बेहतर हो, अगर हम मौक़ापरस्ती से बाज़ आकर दुनिया के तमाम वंचितों और पीड़ितों और दुखियारों को एक नज़र से देखें, और एक ही भावना से उनके बारे में बात करें। अगर वैसा नहीं है तो यह ज़हनी बेइमानी कहलाएगी।
साभार – सुशोभित