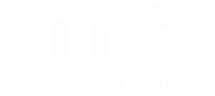मनोज बाजपेयी ने फ़िल्म अलीगढ़ में जैसी देहभाषा (Body Language) प्रस्तुत की, उसके बारे में इधर निरन्तर सोचता रहा। अलबत्ता मैंने बहुत फ़िल्में नहीं देखी हैं- और समकालीन सिनेमा तो और भी कम- फिर भी मुझे याद नहीं आया मैंने हिन्दी सिनेमा में इससे पहले किसी पुरुष-अभिनेता की वैसी भाव-भंगिमा कब देखी थी।
ये एक अजीब तरह से करुण और स्पर्श-कातर देहभाषा थी। समलिंगी-सम्बंधों के परिप्रेक्ष्य में- कह लीजिये किंचित स्त्रैण भंगिमा (Feminine posture) लिये- जो अपनी निजता के सार्वजनिक हो जाने से निहायत एम्बैरेस्ड (लज्जारुण) है। चूँकि वो एक्टिविस्ट-प्रजाति का व्यक्ति नहीं है और शायद एक परम्परावादी मराठी ब्राह्मण ही अधिक है, इसलिए उसमें अपनी इस स्वेच्छाचारिता के लिए ग्लानि भी है। उसे न्याय के संघर्ष में खींच लिया गया है, तब वह आधे मन से वहाँ उपस्थित रहता है। वैसा व्यग्र, एन्क्षस, असहज, सकुचाया चेहरा मैंने तो हिन्दी सिनेमा में नहीं देखा।
पहले मैं सोचता था कि अच्छा अभिनेता वो है, जो अपने पार्ट को भली प्रकार अभिनीत कर लेता है। अगर वो किंचित नाटकीयता के साथ उसे निबाह ले जाये, तब तो और अच्छा। धीरे-धीरे, समय के साथ, जब दुनिया-जहान का सिनेमा देखा और आला दर्जे के अभिनेताओं के काम का साक्षी बना तो ये धारणा भीतर थिर हुई कि अच्छा अभिनेता वो होता है, जो अपनी देहभाषा को जाने कैसी मद्धम आँच पर सिंकाकर पात्र के अनुकूल ढाल लेता है, किंतु वैसा वो सायास नहीं करता। इसके लिए वो अपनी स्मृति, अवचेतन, अनुभूतियों और सृष्टि ने उसको जैसा शरीर दिया है- विशेष तौर पर मुखमण्डल- उसको उस विशेष प्रयोजन के लिये पुकारता है और उस व्यक्ति को वहाँ सम्भव करता है।
जब वो वैसा करने में सक्षम हो जाता है, तो- अगर फ़िल्म दत्तचित्त होकर बनायी गयी है और उसके माध्यम से एक ऐसा स्पेस परदे पर रचा गया है, जो सार्वजनिक होकर भी निहायत निजी है- तो उस अभिनेता का काम वहाँ देखते ही बनता है। देखकर तसल्ली मिलती है। आप सिनेमाघर से कुछ लेकर लौटते है, जो कि बड़ा ज़ाती क़िस्म का कलात्मक संतोष है। आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि बात बन गई थी, और आपने एक ऐसी चीज़ को जीया, जो ख़ूब पकी थी।
नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने फ़िल्म स्पर्श में वो किया था। उन्होंने उस फ़िल्म में एक विशिष्ट बॉडी-लैंग्वेज अर्जित कर ली थी, जिसमें वो बिना अतिरिक्त प्रयास किये स्थिर रह सकते थे, अलबत्ता कोई और उसे भरपूर कोशिशें करके भी छू नहीं सकता था। लंचबॉक्स में फिर यही इरफ़ान (Irfan Khan) ने किया। और अलीगढ़ में मनोज बाजपेयी ने। हिन्दी सिनेमा में ये तीन अभिनय-प्रयास मुझे विशेष रूप से याद रह गये हैं।
फिर वासेपुर के हिंस्र, बनैले पुरुष के तीनेक साल बाद अलीगढ़ (Aligarh) में वैसा एम्बैरेस्ड स्त्रैण चेहरा सामने रख देना- ये तो और कमाल है। इस जक्स्टापोज़िशन- यानी जिसमें दो मुख़्तलिफ़-स्वरूप एक-दूसरे के सामने कुछ वैसे रख दिये जाये कि उनसे एक तीसरी ही रौशनी उभरकर सामने आये- की बिनाह पर आप निश्चित कह सकते हैं कि इस अभिनेता में कुछ तो बात है, जो सबमें नहीं।