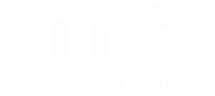राजकुमार राव (Rajkumar Rao) ने एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। उन्होंने एक ऐसे नवयुवक की भूमिकाओं में- नायक या सह-नायक के रूप में- स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो कदाचित् किसी छोटे शहर या क़स्बे से आया है और अब दुनिया में जगह बनाने के लिए जूझ रहा है। आज देश के करोड़ों नौजवान इस वर्ग से वास्ता रखते हैं, राजकुमार उन सभी का प्रतिनिधि-नायक बनता जा रहा है।
ये जो एक दुनिया से दूसरी में आने के कारण निर्मित अंतराल है, उससे राजकुमार के अभिनय में एक ख़ास क़िस्म का खिंचाव उभर आता है। उनके द्वारा निभाए चरित्र एक नर्वस-एनर्जी से भरे रहते हैं। वो हमेशा स्ट्रेच्ड-आउट मालूम होते हैं, अन्यमनस्क और हकबकाये-से। आप देख सकते हैं कि ये युवक अभी तक अर्बन-कल्चर में घुल नहीं सका है, या मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाया है, लेकिन उसकी कोशिश में भरसक जुटा है।
एक तरह की डायरेक्ट-एप्रोच आपको राजकुमार के अभिनय में दिखती है- वो फ़िलॉस्फ़र या शायराना क़िस्म का नायक नहीं है, ना ही बहुत भव्य व्यक्तित्व का स्वामी होने के कारण वो हमें महानायकों की तरह प्रभावित या आक्रान्त करता है- लेकिन अपनी क़स्बाई-ऐंठ, ज़िद, और बेलाग हावभाव के चलते- लगभग ढिठाई से- अपनी डार पर टिके रहने का शिल्प अपने अभिनय से राजकुमार विकसित कर चुके हैं।
फ़िल्म क्वीन में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने राजकुमार राव के द्वारा निभाये गये चरित्र पर टिप्पणी की थी- "मैं उससे ज़्यादा गुड-लुकिंग हूँ, वो तो किसी बस-कंडक्टर के जैसा लगता है!" अब ये वाक्य अपने अभिप्राय में चाहे जितना रेसिस्ट या सेक्सिस्ट हो, फ़िल्म के भीतर राजकुमार के द्वारा निभाये गये सेमी-अर्बन चरित्र पर वो भरपूर टिप्पणी करता है। क्वीन के लिये कंगना की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन राजकुमार ने कुछ ही दृश्यों में परफ़ेक्ट-नोट्स हिट कर लिये थे।
राजकुमार ने अपने अभिनय से ऑलरेडी अपने लिये वो दृश्य रच लिये हैं, जिन्हें आप 'टिपिकल-राजकुमार-राव-सिचुएशन्स' (typical-Rajkumar-rao-situations) कह सकते हैं। मसलन, फ़ज़ीहत में पड़ जाना, बुरे फॅंसना, उलझन में आना, शर्मिंदा कर देने वाले हालात में ख़ुद को पाना, और इसके बावजूद- झेंपते हुए ही सही या ख़ुद को जायज़ ठहराते हुए- एक तरह की ढिठाई से चित्र में बने रहना।
ऐसे दृश्यों में उभरने वाली बेचारगी को- जो उनके चेहरे के विशेष प्रकार के प्रोविंशियल-विन्यास के कारण निखर आती है- राजकुमार अपनी रेपर्टरी (Repertory) का एक ज़रूरी हिस्स बना चुके हैं। अक्सर उनकी फ़िल्में देखकर लगता है कि फलाँ दृश्य को उन्हें सोचकर ही लिखा गया होगा।
मसलन, फ़िल्म न्यूटन में नक्सल-प्रभावित गाँव में देहातियों को मतदान करने के लिये अच्छी तरह प्रशिक्षित कर पाने के अपने मंसूबे के नाकाम रहने के बाद उसका अपनी मेज़-कुर्सी पर सिमटकर बैठ जाना और भीतर ही भीतर घुटते रहना- ये जो सल्किंग-एक्सप्रेशन है, ये राजकुमार पर ख़ूब फबता है। या क्वीन में उसका कंगना की चिरौरी करते रहना- पहले दिल्ली और फिर एम्सटर्डम में- दो अलग शैलियों में। या शादी में ज़रूर आना में उसका सख़्त अफ़सर दिखने का प्रयास करने के बावजूद नर्वस मालूम होना- ये वो तत्व हैं, जिनकी हिन्दी सिनेमा को बड़ी ज़रूरत थी।
वासेपुर, अलीगढ़, स्त्री, बरेली, डॉली आदि फ़िल्मों में ऐसे अनेक प्रसंग आये हैं, जिन्हें आप 'राजकुमार-राव-सिचुएशन्स' कह सकते हैं। इन्हें देखकर आपको उन पर तरस आता है या हँसी आती है, पर वो इन्हें एक मिडिल-क्लास-सेंसेटिविटी (Middle Class Sensitivity) के साथ निबाहते हैं और दर्शकों से वांछित प्रतिक्रिया पाने को अपनी सफलता ही समझते होंगे। उनके पास देश के व्यापक मध्यवर्गीय-युवक-वर्ग की देहभाषा है।
सबसे बड़ी बात- इरफ़ान, नवाज़, मनोज बाजपेयी, केके मेनन के विपरीत उन्होंने और आयुष्मान ने एक ऐसे समय में हिन्दी सिनेमा में पदार्पण किया, जब नये तरह का सिनेमा बनाया जा रहा था और दर्शक नई चीज़ों के लिये तैयार थे। इसलिए वो अपनी भरपूर-जवाँ उम्र में वे सब कर रहे हैं, जो करने के लिए इरफ़ान, नवाज़, मनोज, केके को दस-पंद्रह साल तक समान्तर भूमिकाओं (Parallel Roles) में खटना पड़ा था- एक तरह से अपने लिये दर्शकों को तैयार करना पड़ा था। उनकी बोई फ़सल आज राजकुमार जैसे नौजवान काट रहे हैं- और अभी तो इन्होंने काम शुरू ही किया है।