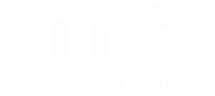विल स्मिथ की फ़िल्म ‘द परस्यूट ऑफ़ हैपीनेस’ (The Pursuit of Happiness) को उसका यह शीर्षक एक राजनैतिक दस्तावेज़ से मिला है। ‘द यूनाइटेड स्टेट्स डेक्लेरेशन ऑफ़ इंडिपेंडेंस’ में इसे थॉमस जैफ़रसन ने लिखा था। जैफ़रसन का मत था कि जीवन, स्वतंत्रता और ख़ुशी की तलाश मनुष्य को ईश्वर-प्रदत्त अधिकार हैं, जिनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ये सच है कि हर प्राणी को जीवन का अधिकार है।
स्वतंत्रता नामक शब्द भी एक राज्यसत्ता के परिप्रेक्ष्य में नागरिक-अधिकारों को ध्वनित करता है। लेकिन ख़ुशी की तलाश? पता नहीं जैफ़रसन क्या सोच रहे थे, जो एक राजनैतिक दस्तावेज़ में उन्होंने ख़ुशी की तलाश (द परस्यूट ऑफ़ हैपीनेस) जैसे वाक्य का इस्तेमाल किया! क्योंकि ख़ुशी एक फ़िलॉस्फ़िकल-कनोटेशन (Philosophical-Connotation) है- कोई जानता नहीं कि ख़ुशी क्या होती है, कैसे मिलती है- उसकी तलाश भले सभी करते हों किंतु सरकारें इसमें आपकी मदद नहीं कर सकतीं। हद से हद वो इतना ही कर सकती हैं कि आपको मायूस ना होने दें- सड़क बना दें, बिजली मुहैया करा दें, अस्पताल चाक-चौबंद कर दें, रोज़गार के अवसर रच दें। ग़ुरबत के ग़म या दु:ख के दलिद्दर कम करना सरकारों का काम है, ख़ुशी देना नहीं- अलबत्ता इंसान के ज़ेहन में ये चीज़ें इतनी आसानी से श्रेणीकृत नहीं होतीं।
यह फ़िल्म अमेरिकन-ड्रीम के प्रतिनिधि नायकों में से एक क्रिस गार्डनर पर आधारित है, जिन्होंने दु:खों और अभावों का जीवन बिताते हुए कालान्तर में सफलता पाई। अपने जीवन-अनुभवों को उन्होंने एक आत्मकथात्मक किताब (Autobiographical book) में दर्ज किया, जिस पर यह फ़िल्म बनाई गई। अमेरिकन सिनेमा का एक बड़ा हिस्सा किन्हीं किताबों पर आधारित है, क्योंकि अच्छे सिनेमा की बुनियाद श्रेष्ठ, ओरिजिनल और जेनुइन कंटेंट होता है, जो इस तरह की किताबों, जिनमें नॉवल्स और पर्सनल-मेमॉयर्स की भरमार है- से प्राप्त होता है।
क्रिस गार्डनर की भूमिका विल स्मिथ ने निभाई। यह 1981 का सैन फ्रैंसिस्को है, जिसमें क्रिस गार्डनर ने अपनी तमाम जमापूंजी एक पोर्टेबल बोन-डेंसिटी स्कैनर की फ्रैंचाइज़ी लेने में ख़र्च कर दी है, लेकिन वो पाता है कि इस डिवाइस की बाज़ार में उतनी मांग नहीं है, जितना कि उसने अंदाज़ा लगाया था। किस प्रकार के मेडिकल-इक्विपमेंट्स कब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेंगे, इसका पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता, अगर लगा पाता तो आज वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ पुख़्ता पूर्व-तैयारी के साथ बाज़ार में मुनाफ़ा कमा रही होतीं। गार्डनर अपने ज़रूरी ख़र्चे पूरे नहीं कर पाता। एक और वैकल्पिक जॉब की तलाश में वो एक स्टॉक-ब्रोकिंग फ़र्म में इंटर्नशिप करने लगता है, जिसमें भविष्य में शायद कभी पैसा मिले, किंतु अभी तो उसे अपना जीवन गुज़ारने के लिए रोज़ संघर्ष करना होगा।
किंतु क्या क्रिस गार्डनर ही ख़ुशी की तलाश कर रहा होता है? आप पूछ सकते हैं कि फ़िल्म का शीर्षक ख़ुशी की तलाश क्यों रखा गया है, जबकि पूरे समय क्रिस केवल सम्मानजनक जीवन जीने के रास्ते तलाश रहा होता है, जिसके लिए एक न्यूनतम आमदनी ज़रूरी है। उसकी कोशिश है कि अपने घर में मेज़ पर बैठकर भोजन कर सके, कल भी भोजन मिल सकेगा यह सुनिश्चित कर सके, अपने बिल्स चुका सके, बच्चे की सालगिरह पर उसे बास्केटबॉल तोहफ़े में दे सके, अपने कमरे में सो सके। बहुतों के लिए यह ख़ुशी की परिभाषा नहीं होगी, बशर्ते आप चीज़ों को पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर, हो सकता है आज बहुतों के लिए जीवित रह पाना ख़ुशी की बात हो। अच्छे से साँस ले पाना, परिजनों का स्वस्थ और सुरक्षित होना, घर से बाहर निकले बिना एक और दिन सफलतापूर्वक बिता देना- आज से दो साल पहले ये ख़ुशी का सबब नहीं था, लेकिन शायद आज है। तब ख़ुशी क्या है? यह तस्वीर तो हमारे सामने साफ़ होती चली जा रही है कि ख़ुशी एक रिलेटिव-शै है, वह सापेक्ष है। मोर द रीज़न व्हाय, यह किसी पोलिटिकल डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत कभी इसे मुहैया कराने का वादा नहीं कर सकती है, बशर्ते हुकूमत को झूठ बोलने से ऐतराज़ ना हो।
फ़िल्म में क्रिस गार्डनर अपनी कहानी ख़ुद सुनाता है। इस कहानी को वो अनेक एपिसोड्स में बांध देता है और उनके शीर्षक भी तय करता है। किसी हिस्से का शीर्षक है- बस का इंतज़ार करना। किसी का- दौड़ लगाना (क्योंकि पोर्टेबल बोन-डेंसिटी स्कैनर एकाधिक बार चोरी हो जाता है), किसी का- मूर्खताएँ करना। सबसे आख़िरी में वो कहता है- “मेरी ज़िंदगी के इस हिस्से का नाम है- ख़ुशी।” यह बात वो तब कहता है, जब उसकी इंटर्नशिप पूरी होने पर उसको यह इत्तेला दी जाती है कि बीस इंटर्न्स में से उसका चयन पेड-सर्विस के लिए कर लिया गया है। ये उसकी ज़िंदगी की किताब में ख़ुशी का चैप्टर है, जबकि कुल मिलाकर इतना ही हुआ है कि अब वो अपने ज़रूरी ख़र्चे सहज होकर पूरे कर सकेगा। वो दौड़कर उस चाइल्डकेयर इंस्टिट्यूट में जाता है, जहाँ उसका पाँच साल का बेटा अपने सिंगल-पैरेंट-पापा की मसरूफ़ियतों के चलते पूरा दिन बिताने को मजबूर है, और बेटे से लिपट जाता है। यक़ीनन यह ख़ुशी का मौक़ा है। लेकिन वो ख़ुशी की तलाश कर रहा था या ख़ुशी उसको मिल गई है? ज़िंदगी में ख़ुशी आपकी परस्यूट होती है, या वह आपका हासिल होती है? और अगर होती है तो कैसे होती है?
अनेक अमेरिकी समालोचक इस बात को समझने से चूक गए हैं। कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं, जो क्रिटिक्स की चहेती होती हैं, वहीं कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं, जिन्हें दर्शक सिर-आँखों पर बैठाता है। ‘द परस्यूट ऑफ़ हैपीनेस’ दर्शकों की प्रिय फ़िल्म है, लेकिन क्रिटिक्स को यह इतनी पसंद नहीं आई। वो इस बात को समझ नहीं सके कि एक आदमी, जो ज़िंदगी में किसी गहरे प्रयोजन या अर्थवत्ता की तलाश नहीं कर रहा, अपने ज़रूरी ख़र्चे पूरे कर सकने के लिए आमदनी के स्रोत भर ही खोज रहा है, उसकी कहानी में वैसा क्या है, जिसे अधिक महत्व दिया जाए? अलबत्ता फ़िल्म मनोरंजक और मार्मिक है इसे सभी समालोचकों ने एक स्वर से स्वीकारा है। वो इस बात को समझ नहीं सके कि ज़िंदगी एक गुंथी हुई पहेली है, वो सरलता से अपने मायनों को नुमायां नहीं करती। बाज़ दफ़े ऐसा भी होता है कि रोज़ी-रोटी के लिए वैसी दौड़धूप से जीवन में एक प्रयोजन-भावना चली आती है, मनुज के मन को उससे भी सुख मिलने लगता है- आवेग वाला सुख नहीं, गुंथ जाने की तल्लीनता। सुख उन तमाम मुसीबतों में नहीं है, सुख मन के वैसे जुड़ जाने में है, जिसमें तसल्ली का एक तरन्नुम उभर आता है- कि मैं तैरकर दूसरे किनारे जा लगा!
फ़िल्म में भीड़ का एक रेला अनेक अवसरों पर दिखलाया जाता है। एक अवसर पर क्रिस गार्डनर महसूस करता है कि उसके सिवा भीड़ में शामिल सभी ख़ुश हैं, मुस्करा रहे हैं, ज़िंदगी से मुतमईन हैं, एक वो ही फ़िक्रमंदी में डूबा है, ग़मे-दौरां उसे खाए जाता है, फ़ाकाक़शी के मंज़र उसको मुँह चिढ़ाते हैं। फ़िल्म के आख़िरी दृश्य में वह ऊष्मा से भरा एक ऊर्जस्वित चेहरा लिए भीड़ के बीच से उभरता है- तब वह उन तमाम लोगों से ज़्यादा ख़ुश मालूम होता है। इस ख़ुशी में एक राहत तो है ही कि अब उसको किसी मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में रात बिताते समय अपने बेटे से यह झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि उसकी पोर्टेबल डिवाइस एक टाइम-मशीन है, जिसने उनको अतीत की किसी सुदूर सदी में पहुँचा दिया है, और अभी वो एक गुफा के भीतर सो रहे हैं- बनैले पशुओं की आहट से ख़ाइफ़ और चौकन्ने। किंतु इस ख़ुशी में आत्मतुष्टि की एक भावना भी है, जो ख़ुद को साबित कर देने पर मिलती है, जब आप जायज़ तरीक़ों से ज़िंदगी में मेहनत और लगन से अपना एक मुक़ाम बनाते हैं और इसका फल आपको मीठा लगता है। तसल्ली में भी एक क़िस्म की ख़ुशी होती है, अलबत्ता ख़ुशी क्या होती है, यह भला कौन जान पाया है?
जिस ‘द यूनाइटेड स्टेट्स डेक्लेरेशन ऑफ़ इंडिपेंडेंस’ से फ़िल्म को उसका यह शीर्षक मिला है, उस पर युवल नोआ हरारी ने अपनी किताब ‘सेपियन्स’ में पूरे दो पन्ने ख़र्च किए हैं और उसने यह साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह से मनुष्य वैसे काल्पनिक-मूल्यों में विश्वास रखता है, जो वस्तुस्थिति में कहीं भी मौजूद नहीं हैं। ‘डेक्लेरेशन ऑफ़ इंडिपेंडेंस’ में स्रष्टा, ईश्वर की कृति, समानता, अधिकार, स्वतंत्रता और ख़ुशी जैसे शब्द आते हैं। हरारी कहता है- कहीं पर कोई स्रष्टा नहीं है, हम किसी ईश्वर की कृति नहीं हैं, हम एवॅल्यूशन की एक प्रयोजनहीन प्रणाली के तहत एवॉल्व हुए हैं, सृष्टि में समानता कहीं नहीं हैं उलटे भिन्नताएँ हैं, अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती केवल वृत्तियाँ और क्षमताएँ होती हैं जो समय के साथ म्यूटेट होती रहती हैं, और ख़ुशी? ख़ुशी को मापने का कोई फीता आज तक साइंस ने ईजाद नहीं किया, हाँ सुख को ज़रूर न्यूरोसाइंस के किन्हीं मानदण्डों पर परखा जा सकता है।
फिर भी ख़ुशी होती तो है- ख़ुशी क्या होती है ये भला कोई मालूम ना कर सके। शायद सबके लिए ख़ुशी के अलग-अलग मायने होते हैं। क्या हम ख़ुशी की तलाश करते हैं? शायद हम उन चीज़ों की तलाश करते हैं, जिनसे हमें लगता है कि ख़ुशी मिल सकती है, लेकिन उन्हें पाकर हम हमेशा ही ख़ुश हो जाएं यह ज़रूरी नहीं है। कितने मज़े की बात है कि ‘द परस्यूट ऑफ़ हैपीनेस’ में क्रिस गार्डनर ख़ुशी की तलाश नहीं कर रहा था। इसके बावजूद ख़ुशी उसको हासिल हो जाती है और जब ऐसा होता है तो धूप में उसका चेहरा गर्वदीप्त होकर चमचमाने लगता है- एक ऐसा चेहरा जो कभी झूठा अहसास बयां नहीं कर सकता।
“दिस पार्ट ऑफ़ माय लाइफ़, दिस लिटिल पार्ट, इज़ कॉल्ड हैपीनेस!”- ख़ुशी का एक आदमक़द चित्र खींच देने वाले वैसे वाक्य सिनेमा में कम ही आए हैं। जिन्होंने यह फ़िल्म देखी है वो इस बात को बेहतर तरीक़े से समझ सकेंगे। और जिन्होंने नहीं देखी वो शायद यह पढ़कर देखने की कसक से भर जाएँ, फ़ौरन से पेशतर उसे देख लेना चाहें!